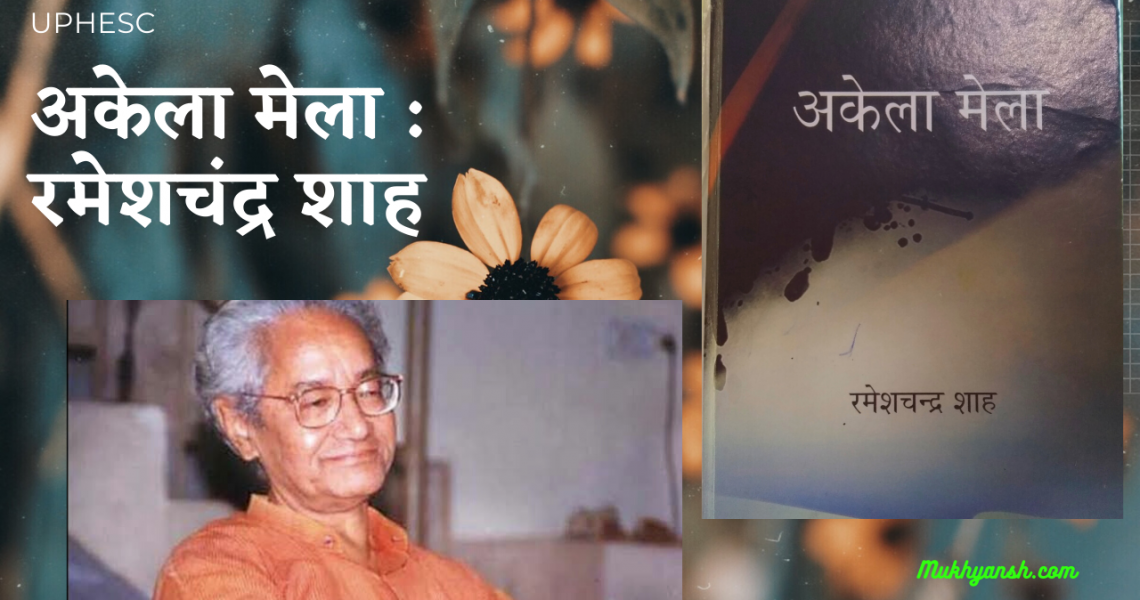(अकेला मेला : रमेशचंद्र शाह)
●दुःख दग्ध जगत् और आनंदपूर्ण स्वर्ग, दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। (जयशंकर प्रसाद)
●एलियट ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी कि अपने व्यक्तित्व से उबरना चाहने का, यानी इस उबरने की छटपटाहट का एक कवि के लिए क्या अर्थ होता है, यह वही जान सकता है जिसके पास व्यक्तित्व हो। जितना समृद्ध और जितना शक्तिशाली वह व्यक्तित्व होगा।
●मनुपुत्र को निश्शंक भाव से इड़ा के हाथों में सौपने वाला कवि जिस ‘मननशील और निर्भय कर्म’ के विश्वास से प्रेरित है, वह न तो यूरोपीय ‘डिसइनहेरिटेड माइंड’ का इच्छित-चिंतन है, न उधारखाते का प्रगतिवाद। (जयशंकर प्रसाद के लिए)
●जान-पहचान के लोगों से कतराकर निकल जाना आसान नहीं होता।
●पुस्तक में उल्लेखित मिनोचा साहब का कथन- भारत का शिक्षक वर्ग सिर्फ वेतन बढ़वाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करता है और, वह भी एक ही पार्टी के झंडे तले । इससे ज़्यादा शर्मनाक और आत्महीन आचरण क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता। आपका वेतन चाहे जितना बढ़ जाए, अपने समाज में आपको वह रुतबा कभी हासिल नहीं होगा, जो अफ़सरों या विधायकों-सांसदों और मंत्रियों को हासिल है। सारे मूल्य-विपर्यय की जड़ में अपना यह सामाजिक-आर्थिक ढाँचा है जो असमानता पर ही टिका हुआ है और उसी का पोषण करने वाला है। समाजवादी साम्यवादी सारे नारे खोखले हैं।
●निर्मल वर्मा ने कहा- कवि या उपन्यासकार को तो यह हक है कि वह जिसे पसन्द न करे। उसे न पढ़े। मगर आलोचक को यह छूट नहीं है।
●यह सवाल खड़ा किया कि क्या कारण है कि बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध की महत्त्वपूर्ण कविता तो अपने समय की सारी बौद्धिक उथल-पुथल को प्रयोगशीलता के बूते घुला सकी, पचा सकी अपनी नई से नई और जटिल से जटिल संरचनाएँ खड़ी करके। जैसे एलियट का ‘वेस्टलैंड’ या पाउंड का ‘कैंटोज़’ “मगर आज सदी के उतार पर, जब जानकारियों का आतंक कई गुना बढ़ता जा रहा है, तब उसका वैसा जवाब दे पाने में कविता अक्षम प्रतीत हो रही है। (निर्मल वर्मा ने लेखक से कहा)
●बड़ी बौद्धिक घटनाओं से बड़ी साहित्यिक प्रतिभाएँ एक उपजाऊ रिश्ता बना लेती है। मगर आज बड़े विचारों का युग नहीं है, छिटपुट शोध-सनसनियाँ हैं विज्ञान की या फिर टुच्ची राजनीति है। दर्शन भी सिकुड़ता गया है और काव्य भी।
●निर्मल जी का यह भी कहना है कि- ‘कला-रूप’ तो वैश्विक होते हैं; किंतु कलात्मक सत्य नहीं। वे विशिष्ट भाषा में ही अवतरित-साकार होते हैं। इसलिए इस भाषा की रक्षा करनी होगी, यदि हमें अपने इस विकराल समय में कला और मनुष्य की गरिमा को बचाए रखना है तो।
●एक संपूर्ण आत्मा होती है और एक आंशिक ‘मैं’ । उन्मेष के क्षणों में जो संपूर्ण है, वही अपने अंश पर उतर आता है। उसे आविष्ट कर लेता है-वह समग्र, जिसमें हमारे सारे अनुभव और संस्कार समवर्ती होकर हमारी पहुँच में आते हैं। (अज्ञेय कहते हैं)
●अज्ञेय के शब्दों में- जीवमात्र की किसी भी अनुभूति के साथ एक जो वृत्त-संरचना अपनी गूंज और अनुगूंज देती है, वह हर किसी के जीवन में हर घटना के साथ अलग होती है। साहित्यकार जो एक-सा है, उसे आधार मानकर, उस पर खड़े होकर, जो हर चरित्र के लिए अद्वितीय है, उसकी पहचान करता है। जिसको वह पहचान होती है, वह भी उस पहचान के बाद थोड़ा बदल जाता है।
●अज्ञेय स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र और नृतत्त्व के अध्ययन ने संस्कृति पर परंपरा के बारे में हमारे चिंतन को काफ़ी विस्तार दिया है। मार्क्सवादी चिंतन के साथ इन क्षेत्रों में जो गैर-मार्सी चिंतन हुआ है, वह भी हम तक पहुँचता रह सका है। अपना अनुभव बताते हुए वे कहते हैं, “स्वयं अपनी बात कहूँ तो इस संबंध में मार्क्सवादी चिंतन को अपर्याप्त मानकर ही मैंने दूसरी दार्शनिक परंपराओं का भी अध्ययन किया और फिर उन सबको एक तरफ रखकर भारतीय चिंताधाराओं से परिचय पाने का भी प्रयत्न किया।”
●इस पुस्तक में मनुभाई पंचोली का कथन- उन्होंने गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों को दो हिस्सों में बाँटा। एक, काल-सार्थक विचार और दूसरा, कालातीत शाश्वत उपयोगिता का विचार । असत्य संगठित हो तो भी उसकी पराजय अंततः निश्चित है; किंतु सत्य को भी संगठित होना चाहिए, तभी उसकी विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा उन्होंने एक पाश्चात्य विचारक (यहूदी प्रोफ़ेसर) के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा।
●मनुभाई का कथन- जटिलता जितनी मात्रा में बढ़ती है, उसी अनुपात में सच्ची सरलता का ‘इम्पैक्ट’ पड़ने की संभावना भी बढ़ती जाती है।
●गाँधी जी का कथन- इस देश का कठोर हृदय बुद्धिजीवी मेरे जीवन का सबसे लंबा दुःस्वप्न रहा है। यही सब समस्याओं की जड़ है।
●महात्मा गाँधी के ‘हिंदी स्वराज’ को विद्यानिवास मिश्र ने “भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज ग्रन्थ (या मेनिफेस्टो) कहा है।
●रमेशचन्द्र शाह लिखते हैं- मेरे ख्याल से श्री अरविंद का ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर’, जो एक बहुत भिन्न ढंग से लिखी गई पुस्तक है, वह भी इस श्रेय की हकदार है। ‘हिंद. स्वराज’ के परिपूरक-सी।
कुछ मुद्दे इस बीज ग्रंथ के :
- हमारी स्थितिशीलता गुण है, दोष नहीं। अनुभव से हमें जो ठीक लगा है, उसे हम क्यों बदलेंगे ?”बहुत-से अक्ल देने वाले आते-जाते रहते हैं। पर हिंदुस्तान अडिग रहता है। यह उसका लंगर है।
- ऐसी सभ्यता जहाँ हो, वहाँ जो आदमी फेरफार करेगा, उसे आप दुश्मन समझिए।
- जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं, उन्हें हम पहचानते नहीं, न वे हमें पहचानते हैं।
- अंग्रेज़ अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है।
- उपर्युक्त पर आपत्ति उठाते हुए जब ‘पाठक’ कहता है, “अंग्रेज़ हिंदुस्तानी बनें, यह नामुमकिन है” तो यह ‘संपादक’ कहता है, “हम पहले अपना घर साफ रखें। फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे। दूसरे अपने आप चले जाएँगे।” यह भी कि “हमने उनकी सभ्यता अपनाई है इसलिए वे यहाँ रह रहे हैं।”
जब पाठक ‘तवारीख़’ की दुहाई देता है, संपादक कहता है, “हिंदुस्तान का बल दूसरे किस्म का है, असाधारण है। इसलिए दूसरी ‘तवारीखों’ से हमारा कम संबंध है।” - भाषा को लेकर गांधी जी की यह बात आज कितनी कारुणिक और भयानक विडंबना से भरी लग उठती है !
-हमारे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेज़ी। और ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा।
-अंग्रेज़ी शिक्षा पाए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी नहीं उठा रखा। अगर आज हम अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो हम पर उसका जो कर्ज चढ़ा है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा अदा करते हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं, हमीं पर पड़ेगी।
- धर्म को लेकर, “हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक पनप नहीं सकते।” तथा …”धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी हैं।” ये दो बातें एक साथ गांधी जी ही कह सकते थे ।
- एक अद्भुत रूपक, “हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ़ होना है। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं।”
- गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट जाएगा। लेकिन अनीति से पैसे वाला बना हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा।
- अंग्रेज़ों से, “अगर आप अपनी सभ्यता को, जो सचमुच बिगाड़ करने वाली है, छोड़कर अपने धर्म की छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा, हमारी माँग ठीक है। उस ढंग से आप रहेंगे तो हमें जो थोड़ा सीखना है, वह हम आपसे सीखेंगे और हमसे आपको जो सीखना है, वह आप सीखेंगे। मगर यह तभी होगा जब हमारे संबंध की जड़ धर्मक्षेत्र में जमे।
●रमेशचंद्र शाह मानते हैं कि अज्ञेय पर ‘गुर्जियेफ़’ का खासा प्रभाव पड़ा होगा युवावस्था में।
●गुर्जियेफ़ के कथन का रमेशचंद्र शाह द्वारा हिंदी अनुवाद है यह-
●खारा नहीं चाहते तो माधुर्य भी नहीं मिलेगा।
●वह रसातल में है। इसलिए कि तुम शिखर पर हो।
●अगर कोई आदमी कायर है तो इससे साबित होता है, उसमें इच्छाशक्ति का अभाव नहीं।
●सत्य वह चीज़ है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संकटों से सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है।
●अँधेरे में एक जूं तक बाघ से ज़्यादा डरावनी हो जाती है।
●जिसका व्यक्तित्व आत्म-चेतस् है, उसे न ईश्वर की ज़रूरत है, न शैतान की।
●सुखी है वह मनुष्य, जिसे अपने ‘असुख’ की चेतना नहीं, ख़बर नहीं।
●आग पानी को खौला सकती है; पर पानी आग को बुझा सकता है।
●अगर तुम पहले नंबर पर हो, तो तुम्हारी पत्नी दूसरे पर रहेगी। अगर पत्नी को प्रथम रहना है, तो बेहतर है, तुम अपने को सिफ़र बना लो। तभी घर में चैन रहेगा।
●प्रसिद्धि की दरकार है तो पत्रकारों से दोस्ती करो। चैन की नींद चाहिए तो पत्नी से दोस्ती गाँठो। अपनी धार्मिक आस्था खोने की इच्छा हो तो पादरियों से दोस्ती करो।
●स्वप्न में कुछ भी न तो असंगत लगता है, न असंभव । क्षण-मात्र में पूरा दिन बीत जाता है बल्कि बरसों बीत जाते हैं। समय का, और जगह का, दूर-पास का कोई मतलब नहीं रहता। सब कुछ सब जगह एक साथ मौजूद है। और अगर वह सब अनर्गल है, ‘ऐब्सर्ड’ है तो इसकी क्या गारंटी है कि जागृति की दुनिया जैसी हमारी इंद्रियों को और मन को भासती है, वही सत्य है ? सपना देखने वाली भी हमारी चेतना है और जागृति का जीवन भी चेतना का ही खेल है तो कौन-सा खेल सच मानें ? या फिर ये दोनों ही सच नहीं हैं और सच चेतना की कोई तीसरी या चौथी अवस्था है?
●यूँ निर्मल जी इतने शालीन स्वभाव वाले हैं कि जिसे सचमुच नापसंद करते हैं, उसे भी महसूस नहीं होने देंगे कभी अपनी असुविधा। मगर, मुझे लगता है, उस ‘दूसरे’ को तो महसूस कर ही लेना चाहिए कि वह विघ्न पहुँचा रहा है, उनके एकांत में। ख़ासकर, जब वह दूसरा स्वयं एक लेखक है।
●निर्मल वर्मा ने एक लेख में लिखा है-
1. मनुष्य क्या है, इस प्रश्न को अनेकानेक स्तरों पर सभी विधाओं में उघाड़ा गया। किंतु व्यक्ति क्या है, इस प्रश्न के साथ पहली मुठभेड़ उपन्यास ने ही की। उपन्यास की पीड़ा व्यक्ति की प्रसव-पीड़ा है।2.हेगल ने उपन्यास को आधुनिक मध्यवर्ग का महाकाव्य कहा । पर जिस समूचे मनुष्य की विराटता को ‘ऐपिक’ कहते थे, वह बुर्जुआ समाज तक आते-आते खंडित व्यक्तित्वों में इतने भयानक ढंग से बिखर गया है कि उपन्यास उसे केवल नॉस्टेल्जिक क्षणों में पकड़ पाता है।
3. उपन्यास पूर्णतः सेकुलर विधा है। यहाँ सब कुछ व्यक्ति के स्वायत्त, स्वेच्छाचारी निर्णयों पर निर्भर है
4. व्यक्ति के इस अराजक संसार का तर्क काफ्का में चरम तक पहुँचता है। वह अंतिम उपन्यासकार था जो मनुष्य की अतिनैतिक ‘एमॉरल’ और सेक्युलर सीमाओं को अतिक्रांत करना चाहता था-एक सर्वव्यापी नियम और प्रेम के वैध संसार में प्रवेश करने हेतु। किंतु वह उस सीमांत पर मार डाला गया। यहीं से ‘उपन्यास की मृत्यु’ का नारा उछला। जो व्यक्ति की मृत्यु की भी घोषणा में परिवर्तित हुआ।
5. स्पेनिश विचारक आर्तेगा गास्से ने यूरोपीय व्यक्ति के ‘मासमैन’ (भीड़ का आदमी) में कायाकल्प कापातरण की प्रक्रिया का साक्षात किया। रेनेसांस-युग के महानायक के विद्रूप सरीखा । दास्ताएवस्की से कामू तक की यात्रा। ‘नोट्स फ्रॉम दि अंडरग्राउंड’ का चरितनायक अपने अंधेरे तहखाने में निर्वासित अजनबी था तो कामू का दिन दहाड़े अपने चरम औसतपन में उघड़ा हुआ।
6.पश्चिमी सभ्यता में व्यक्ति की यह ऐतिहासिक परिणति अनिवार्य थी। इसलिए कि वहाँ ‘ईगो’ (अहं) और ‘सेल्फ’ (आत्मन्) के बीच कभी भी स्पष्ट विवेक उपलब्ध और चरितार्थ नहीं हुआ। यहीं पर सॉल वैलो के उपन्यास ‘हरजोग’ की कुंजी सरीखी अर्थवत्ता उजागर होती है।
7. यूरोपीय उपन्यास की अहं-अक्रांत दुनिया से निकलकर यदि हम मनुष्य के भारतीय संस्करण में-आत्मन्-संस्कार में प्रवेश करें तो हम मानो इकाइयों की दुनिया से निकलकर संबंधों की दुनिया में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ निर्मल की समझ में एक अन्योन्याश्रय की स्थिति है। मनुष्य सृष्टि के केंद्र में नहीं है। वह सिर्फ ‘रिलेटेड’ है। दूसरों से जुड़ा हुआ। वह स्वायत्त इकाई भी नहीं, उस तरह ।
●(अज्ञेय के लिए)– मैंने उनसे यह भी कहा कि वात्स्यायन जी, और किसी के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा। पर आपके बारे में मुझे अकसर लगता है कि काश, आपसे मेरा संपर्क पहले-अपेक्षाकृत युवा दिनों में हो गया होता ! मेरे कवित्व को जगाने के लिए-मुझे अपने ही भाव-जगत् को लेकर आत्मविश्वास प्राप्त करने में-आपकी भूमिका जितनी उत्प्रेरक सरीखी होती, उतनी और किसी की नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं का सही विरेचन सही वक्त पर न हो पाना कितना गाँठ उपजाने वाला होता है।
●पढ़ना भी किसी बहुत गहरी जरूरत और प्रेरणा से ही होता है।
●येट्स हमें बताता है-“जो दुनिया के साथ शांत, किंतु खुद अपने साथ युद्धरत रहते हैं। किंतु दांते ऐसा शख्स था जिसे दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता था।” यहीं पर येट्स की वह सुप्रसिद्ध सूक्ति उभरती है जिसके अनुसार, “जब हम दुनिया से, यानी दूसरों से झगड़ते हैं तो सिर्फ रेटरिक (वाग्मिता) उपजाते हैं और अपने साथ झगड़ते हैं तो कविता रचते हैं।”
●एलियट ने बाकायदा दो बरस हारवर्ड में उस वक्त के इंडोलॉजिस्टों में अग्रणी प्रो० लैनमन से संस्कृत सीखी थी; जबकि येट्स को न केवल संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन का भी उसने वैसा विधिवत् अध्ययन नहीं किया था जैसा एलियट ने।
●अज्ञेय के अनुसार : ”स्वाधीनता ऐसी चीज़ है जो निरंतर आविष्कार, शोध और संघर्ष माँगती है, यहाँ तक कि उस शोध और संघर्ष को स्वाधीनता का सार-तत्त्व कह सकते हैं।” स्वाधीन होना अपनी चरम संभावनाओं की संपूर्ण उपलब्धि के शिखर तक विकसित होना है। पर कोई भी व्यक्ति अपनी चरम संभावनाओं को ऐसे ही परिवेश में पा सकता है जिसमें दूसरे भी अपनी चरम संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए समान रूप से स्वाधीन हों और ठीक यहीं पर स्वाधीनता का ऐसा बोध मानो तपस्या की यंत्रणा बन जाता है, क्योंकि वह मानव-मात्र की समान स्वाधीनता के प्रयत्न की अनिवार्यता बन जाता है। स्वाधीनता की सच्ची कसौटी मैं नहीं, ममेतर है।”
●इतना तो अब स्पष्ट हो चुका है कि विज्ञान हमें जिस ज्ञान को देने का दावा करता है, वह सारतत्व का ज्ञान न होकर मात्र शुद्ध संरचना का ज्ञान है। तब यह कहना कि मनुष्य के लिए और किसी भी प्रकार का ज्ञान सम्भव या उपयोगी नहीं, एकदम झूठा और अनुभव-विरोधी (इसलिए अंततः मानव द्रोही) होगा।
●जयदेव सेठी की पुस्तक पढ़ गया- ‘गाँधी की प्रासंगिकता’। इसके प्राक्कथन में जयप्रकाश जी ने कुछ दो -टूक बातें रखी हैं जो माननीय है-
1. नेहरूई उदारवाद और मार्क्सवाद के प्रभाव में पले-पुसे बुद्धिजीवी हक्के-बक्के हो गए हैं। उन्हें अब ऐसे मॉडल की ज़रूरत महसूस होने लगी है जो स्वदेशी हो, आज की दुनिया का सामना कर सके और भारतीय परंपरा के उत्तम तत्त्वों का इस्तेमाल कर सके-सिर्फ जिनके जरिए ही यहाँ की जनता को राजनीतिक-आर्थिक विकास का साझीदार बनाया जा सकता है।
2. गांधी जी के सही अध्ययन के लिए अंतरशास्त्रीय पद्धति का दृष्टिकोण आवश्यक है। (नई बात है न यह ?)
3. नेहरूई ढाँचा गैर-भारतीय और विशिष्ट वर्गोन्मुखी होने से असफल होना ही था।
4. हमारी राज्य-व्यवस्था व उसकी संस्थाएँ जर्जर कर दी गई हैं। हमारे समाज के नैतिक अंतर्रात्र के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं।
5. हमारी शिक्षा पद्धति में गांधी-अध्ययन का कोई विधान नहीं। क्यों ?
6. सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, सत्याग्रह, समानता व श्रम-रोटी-ये गांधी जी की मूल छह संकल्पनाएँ हैं।
7. गांधी जी ने संपूर्ण मानव-जीवन की चुनौती को समझा। उनकी संकल्पना इस अर्थ में द्वंद्वात्मक भी है कि इसमें व्यक्ति व समाज, सत्ता और आज़ादी, विशिष्ट वर्ग व जन-साधारण, संपत्ति और संपत्तिहीनता, श्रम और पूँजीपति के बीच निरंतर संघर्ष निहित है।
(इस बिंदु पर विवाद हो सकता है कि सेठी कहीं यहाँ अपना अर्थ तो आरोपित नहीं कर रहे हैं गांधी पर ?)
पर, आगे जो वे कहते हैं वह ठीक ही लगता है। नहीं ?8. गांधी जी की द्वंद्वात्मकता दो असाम्यों का संघर्ष नहीं थी। निश्चित आदर्श के प्रतिकूल द्वंद्वों व विरोधाभासों को सत्याग्रह व जनसंघर्षों द्वारा परिवर्तित करने का माध्यम थी।
9. संपूर्ण क्रांति को गांधीवादी अंतर्वस्तु दें, क्योंकि मुझे और किसी विचारधारा में सार नज़र नहीं आता।
10. भारतीय मार्क्सवादी अन्य मार्क्सवादियों से अलग नहीं बन पाए। उनके लिए भी अब जो रास्ता हो सकता है, वह गांधी जी से ही होकर गुज़रता है। न तो रूस, न ही चीन का रास्ता हमारे लिए अनुकूल है।
●ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी नजर में- अपनी अंतरात्मा के सामने जो कुछ है- वैसे ही दूसरों को क्यों नहीं भासते? चाहे हम अपने तईं कितने ही ईमानदार क्यों न हों। दूसरा हमें अपने ही अनुमान, अपनी ही प्रत्याशाओं, अपनी ही अभिलाषाओं के हिसाब से ग्रहण करता है। जैसे हम अपने को दे रहे हैं, वैसे नहीं।
●मगनभाई प्रभुदास देसाई की लिखी पुस्तक ‘राममोहन राय से गांधी जी तक’ पढ़ गया हूँ। कुछ बातें जो पता नहीं थीं, पहली बार इसमें देखीं। कुछ नए सिरे से विचार को उकसाने वाली लगीं।
1. 1924-25 में सकलतवाला की कोशिश गांधी जी को साम्यवादी दल की ओर आकृष्ट करने की। गांधी ने साफ़ जवाब दे दिया-मेरी नीति मौलिक रूप से साम्यवाद से भिन्न है। समाजवादी पार्टी का जन्म, जिसने 1948 तक कांग्रेस में रहकर काम किया।
2. 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने कहा-क़ौमी सवाल और मंदिर-प्रवेश मूलतः आर्थिक सवाल हैं और उसी ढंग से उन पर विचार अपेक्षित। नेहरू मार्क्सवाद से प्रभावित होकर ये बातें कर रहे थे। इस तरह हरिजन, मुसलमान और राजे-रजवाड़े तीनों वर्ग एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े कर दिए गए।
3. स्क्रिप्स प्रस्ताव ‘भविष्य में भुनने वाला गैरमियादी चेक’ । गांधी जी के कथनानुसार। [मेरी शंका : मगर, अरविंद ने इसे स्वीकार लेने का संदेश भेजा था। क्यों, कौन सही था अंततः ?]
4. अंग्रेज़ी राज में मुसलमानों ने अपनी राजनीति में दंगों का एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया।
5. “औरंगजेब के जमाने की इस्लाम की इज्जत को कायदे आज़म ने फिर कायम किया-इस देश के मुसलमान इसके लिए सदा उनके अहसानमंद होंगे।” -मो० शब्बीर अहमद उस्मानी।
6. जीर्णोदयवादी हिंदू राजनीतिज्ञ हिंदू राज्य की बात करते हैं। राजपूतों-मराठों के काल के संकीर्ण हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर। पर इतिहास बताता है, हिंदू धर्म की इस जीवन-दृष्टि ने अंत में देश को गुलाम बनाया। यह एकता-प्रेरक या प्रगतिशील सिद्ध नहीं हुई।
7. गांधी ने हिंदू धर्म की प्राचीन विशालता को जीवित किया। प्रत्यक्ष जीवन-व्यवहार में सिखाया-हिंदू धर्म सनातन शक्ति है। तीस जनवरी भारतीय धर्म के नवयुग का आरंभ है।
●आज बापू की पुण्यतिथि है। पिछले कई दिनों से मैं ‘बापू के पत्र मीरा के नाम’ पढ़ता रहा हूँ। यह पुस्तक मुझे एक अंतरंग दस्तावेज़ की तरह लगती है-गांधी जी के स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने की दृष्टि से। मन हो रहा है, इसमें से कुछ बातें-सूक्तियों की तरह अपने सामने रख-सहेज लूँ :
1. 4 दिसंबर, सन् 1925 के पत्र में वे लिख रहे हैं यह थोड़े दिन का वियोग उस लंबे वियोग की तैयारी है जिसे मृत्यु लाती है। असल में यह वियोग ऊपरी है मृत्यु से हम ज़्यादा नज़दीक आते हैं। क्या शरीर बाधा नहीं है, यद्यपि वह परिचय का साधन भी है ?
2. जिस चीज़ को लेने की हमें ज़रूरत या इच्छा न हो, उसका स्वाद हमें क्यों जानना चाहिए ? क्या तुम्हें मालूम है, हर तरह के पापाचरण को उचित ठहराने के लिए यही दलील दी जाती रही है ? वर्जित सेब का किस्सा।
3. तुम्हें शरीर से मोह हरगिज़ न होना चाहिए। शरीर-रहित आत्मा शरीरबद्ध-दुर्बल जीवात्मा से अधिक है जिसके साथ शरीर की सारी मर्यादाएँ लगी हैं। शरीररहित आत्मा संपूर्ण है और उसी की हमें आवश्यकता है।
4. धार्मिक भावना की सच्ची कसौटी, ‘थोड़ा-बहुत ठीक’ से ‘ज़्यादा ठीक’ चुन सकना।
5. आलोचना के अधिकार के लिए हमें स्पष्ट समझ और पूरी सहिष्णुता की प्रेमशक्ति चाहिए।
6. जो चाहिए सब मिल जाए तो हमारी श्रद्धा का मतलब क्या ?
7. कोई ज़ालिम ऐसा नहीं हुआ जिसे दूसरों को दिए कष्ट का मूल्य न चुकाना पड़ा हो। किसी प्रेमी ने कभी पीड़ा पहुँचाकर उससे कम पीड़ा नहीं सही है। मेरा यही हाल है।
8. दिमाग की मानी हुई सच्चाई को फौरन दिल में उतार लेना चाहिए, नहीं तो वह बेकार जाती है और मवाद बनकर शरीर को विषाक्त कर देती है।
9. सूर्य को थकावट क्यों नहीं ? हम यह क्यों समझें कि उसे आज़ादी नहीं, वह जड़ है। और हमें आज़ादी है। हम स्वयं शून्य बन जाएँ। अपने को उसकी मर्जी पर छोड़ दें।
10. हिंदू जितना अपने धर्म के बारे में आजकल सोच रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं सोचते थे।
11. तारों के साथ सीधा संपर्क निहायत ज़रूरी है। खुले में सोओ। 12. सहमत न हो पाने से आत्मपीड़न करके अपनी विचार-शक्ति को निकम्मी मत बनाओ ।
13. मैं और शून्य को पास-पास रखकर सोचोगी तो तुम्हें दो चिह्नों में जीवन की सारी समस्या समाई दिखाई देगी।
●‘जायसी’, मुझे लगता है, हिंदी आलोचना के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। साही जी के मुख्य सूत्र जो इनमें से उभरते हैं, यूँ हैं-
1. तटस्थ उदारता की दृष्टि ही जायसी की वास्तविक दृष्टि है।
2. भाषा-प्रयोग को लेकर-जायसी के युग में मनुष्य की आंतरिकता को व्यंजित करने वाले यही बौद्धिक मुहावरे थे। और उन्होंने इनका पारिभाषिक नहीं, भावनात्मक उपयोग किया। जिस तरह अज्ञेय ने मनोविश्लेषण का या प्रेमचंद ने वर्गों का।
3. पद्मावती को आध्यात्मिक प्रतीक का दर्जा देना न कथा-प्रबंध का अभीष्ट है, न जायसी की असली तलाश।
4. अब तक की आलोचना में पद्मावती की खोज ने आलोचकों को ‘पद्मावत’ की खोज से विमुख ही किया है।
5. काव्य-कृति, जिसने इतिहास को जन्म दिया। यह क्षमता उसके संपूर्ण अर्थपुंज का महत्त्वपूर्ण अंश है।
6. जायसी ने ट्रेजडी का दर्शन किया-अपने समाज में व्याप्त सत्ता-संघर्ष में। हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के बाद सचमुच एक भारतीय हृदय, एक समाज बन सकेगा या नहीं, यह मथने वाला प्रश्न जायसी यानी सोलहवीं सदी के सामने है।
7. लोहिया के हवाले से देशी-परदेसी के संघर्ष को प्रमुखता दी है साही ने। 8. सारे संघर्ष के बीच उस निर्मल भाव (प्रेम) की तलाश कर रहे थे जायसी। 9. जितना मन का यूटोपिया सिंहल द्वीप, उतनी वीरानगी, जितना प्रेम, उतना युद्ध । अल्लाह-प्रेम के ज्ञान को इतिहास के चक्के पर चढ़ाने की चुनौती।
10. पर इसका क्या अर्थ है कि “जायसी को साधना की नहीं, प्रातिभ आंतरिकता की तलाश थी ?” खुसरो के द्वैत से जायसी को अलग करते हैं साही, कि “उन्होंने इस यूटोपिया को इतिहास के बीचोबीच ला खड़ा किया। यह जो संधिस्थल सिंहल द्वीप और इतिहास का जायसी ने देखा, वह फिर किसी ने नहीं देखा। अपने ट्रैजिक विजन में अकेले हैं जायसी।”
●हर विचार, चाहे वह तथाकथित भीतर से उपजे, चाहे तथाकथित बाहर से, मन और बुद्धि के संतुलन को फिर से डगमगा देता है।
●‘स्वराज इन आइडियाज़’ शीर्षक प्रख्यात दर्शनशास्त्री के०सी० भट्टाचार्य के सन् 1928 में दिए गए अत्यंत विचारोत्तेजक व्याख्यान की साइक्लोस्टाइल्ड प्रति निर्मल जी मुझे दे गए हैं। उनका आग्रह है कि मैं प्रो० के०जे० शाह के ‘फिलोसॉफिकल जर्नल’ के लिए इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी अवश्य लिखू।
व्याख्यान अंग्रेज़ी में दिया गया है। हिंदी अनुवाद में उसके कुछ मुद्दे यूँ होंगे-
1. सांस्कृतिक गुलामी अचेतन स्तरों पर हमें जकड़े रहती है। जिस दबाव या अंकुश के प्रति हम सचेत होते हैं, उसे हम प्रतिरोध दे सकते हैं, झेल सकते हैं और उसके बावजूद अपने अंतःकरण में मुक्त रह सकते हैं। किंतु सांस्कृतिक रूप से पराधीन व्यक्ति को अपनी परवशता का होश ही नहीं होता। तो क्या खाकर वह उसका प्रतिकार करेगा और कैसे ?2. यह सांस्कृतिक परवशता तब उपजती है जब विचारों-भावनाओं का हमारा पारंपरिक साँचा, बगैर किसी स्पर्धा या तुलना के एक विदेशी-विजातीय साँचे द्वारा पूरी तरह विस्थापित और अतिक्रमित कर दिया जाता है। यह विजातीय संस्कृति तब हमसे एक प्रेत की तरह चिपट जाती है। इस प्रेतबाधा से जब हम अपने को पूरी तरह मुक्त कर लेते हैं, तब हमें फिर से नया जन्म लेने जैसी अनुभूति होती है और वैचारिक स्वराज से मेरा आशय यही प्रेत-मुक्ति है।
3. सारा हमारा शिक्षा-तंत्र ही इस समय ऐसा है कि पाश्चात्य संस्कृति ही हमारे भीतर सबसे पहले पैठ जाती है। अपनी प्राचीन संस्कृति को हम इस तरह आत्मसात् नहीं करते। महज़ कुतूहल की तरह उसमें ताक-झाँक भर करते हैं। हमारे शिक्षित लोग वैसा कतई नहीं सोचते-महसूसते, जैसा उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति के निरंतर संपर्क में सोचना-महसूसना चाहिए कि वे इस संपर्क के फलस्वरूप अपनी स्वयं की आत्मा का आविष्कार कर रहे हैं।
4. पाश्चात्य संस्कृति हम पर लादी तो गई किंतु हमने खुद भी उसकी चाहना और माँग की थी। उसे हमने खुली आँखों, खुले होशोहवास से आत्मसात् नहीं किया-अपनी परंपरागत भारतीय बुद्धि के जरिए। वह हमारा परंपरागत मन हम शिक्षित भारतीयों की पहुँच से बाहर हमारी चेतना के अचेतन स्तरों में जा डूबा है। अब वह सिर्फ हमारे कुछ पारिवारिक-धार्मिक रीति-रिवाजों-अनुष्ठानों में ही सक्रिय होता है-पर उन अनुष्ठानों-संस्कारों का भी कोई जीवंत अभिप्राय हमारे भीतर नहीं धड़कता। जब अपनी ही विरासत के साथ हमारे रिश्ते का यह हाल है, तो जो हम पर आरोपित की गई है, उस संस्कृति के जीवंत आत्मसात्करण का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?
5. तथापि ये विजातीय और आरोपित विचार हमारे भीतर घुसपैठ कर एक तरह की आत्महीन विचार-प्रक्रिया को तो उकसा ही देते हैं जो सचमुच के मस्तिष्क की तरह काम करता दिखता है। पर उससे वास्तविक सृजनात्मक आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
6. ऐसी अवस्था में हम अपने ऊपर, अपने बारे में पश्चिमी संस्कृति के पूर्वग्रहप्रेरित फैसलों को ज्यों का त्यों कबूल कर लेते और उन्हीं को दुहराने लगते हैं। या फिर हमारी प्रतिक्रिया नपुंसक नाराज़गी की होती है क्योंकि हममें सचमुच के आत्मालोचन की, अपनी वास्तविक स्थिति के सम्यक् आकलन की क्षमता ही नहीं है।
7. हमारी राजनीति को देख लो-‘शक्ति’ का कोई ‘पर्सेप्शन’ नहीं। हमारे समाज-सुधारकों ने क्या सचमुच कभी इसकी जाँच-पड़ताल की है कि पश्चिम के सामाजिक सिद्धांत क्या सचमुच ऐसे सर्वव्यापी और सार्वभौम सत्य हैं कि आँख मूंदकर अपने यहाँ लागू किया जा सके ? हम चाहे निर्विचार रूढ़िवाद अपनाएँ, चाहे काल्पनिक प्रगतिवाद, दोनों ही मुद्राएँ हमारी नकलची मुद्राएँ होती हैं क्योंकि दोनों जगह हम पश्चिम का ही मुँह ताकते हैं। विद्वता के क्षेत्र में-मैं पूछता हूँ क्या हमने पश्चिमी साहित्य अथवा चिंतन का एक भी ऐसा मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, जिसे हम भारतीय कसौटियों पर कसा गया मूल्यांकन कह सकें ? दर्शन में भी, कोई संश्लेषण नहीं दिखता। एक भी उदाहरण नहीं, जिसे हम भारतीय दृष्टिकोण से किया गया पाश्चात्य दार्शनिक विचारधाराओं का आकलन कह सकें। जबकि असली चुनौती तो यही थी। भारत की आत्मा की खोज की-उसके प्राचीन स्वरूप और इस अधुनातन स्वरूप के बीच कोई एक अविच्छिन्न सातत्य की प्रामाणिक पहचान उपलब्ध करने की। बेशक, महाप्राण प्रतिभा इस भारतीय आत्मा को उद्घाटित कर सकती है; किंतु यह तो अंततः दर्शन की ही ज़िम्मेदारी होती है कि तर्कसंगत पद्धति से उसे खोजकर प्रस्तुत करे।
8. हमारा वास्तविक ‘माइंड’ एक ऐसे ‘शैडो माइंड’ द्वारा बेदख़ल किया गया है जिसकी कोई जड़ नहीं। न हमारे अतीत में, न वास्तविक वर्तमान में। अब, चूँकि उस प्राचीन जातीय चित्त को न तो पूरी तरह पाताल में धकेला जा सकता है, न तो उसकी बाहर से लादी गई सतह है, वही उपजाऊ और असरदार ढंग से काम कर सकती है, अतः इस स्थिति के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। हर जगह मतिभ्रम फैला हुआ है और विचारों का हर क्षेत्र वर्णसंकरता और बाँझपन का शिकार हो गया है। यह मानसिक गुलामी खंजर की तरह हमारी आत्मा तक धंस गई है। सबूत चाहिए तो देशी भाषा और अंग्रेज़ी का घालमेल ही देख लीजिए। सांस्कृतिक विचारों को व्यक्त करना ही हमारे लिए दुस्साध्य हो गया है।
9. प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट रूपाकार-संरचना होती है, जो उस संस्कृति द्वारा प्रस्तुत हर जीवंत विचार और आदर्श में प्रतिबिंबित होती है-अनिवार्यतः ।
10. जीवन का अर्थ ही है-बदलती हुई जगत्-गति और परिवर्तमान आदर्शों के साथ तालमेल बैठाते चलना। किंतु इसके लिए पहले यह अनिवार्य है कि हम इस प्रक्रिया और पद्धति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हों। यहाँ पैबंदों से काम नहीं चलाया जा सकता।
11. इस मतिभ्रम का तत्काल निवारण ज़रूरी है। इसे एक सुनिश्चित टकराव और संघर्ष में परिणत होना होगा। हमें इस घालमेल से उबरना ही होगा। सच्चा संघर्ष तभी संभव है जब हम अपने प्रतिमानों के बारे में गंभीर हों।
12. पाश्चात्य प्रतिमानों के साथ अपने स्वदेशी प्रतिमानों का संश्लेषण करना हर जगह ज़रूरी नहीं है। जहाँ वह ज़रूरी लगे, वहाँ भी प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि पाश्चात्य प्रतिमानों का अनुकूलन-समायोजन हमारे प्रतिमानों द्वारा, हमारे प्रतिमानों के आधार पर हो; न कि इसके उलट।
13. विश्ववाद के पक्ष में तर्क-किसी भी समुदाय और यहाँ तक कि मानव-जाति की ही प्रगति कुछ आदर्शों के क्रमिक सरलीकरण और एकीकरण का प्रतिफल होती है। बुद्धिवाद का, सर्वसामान्य तर्कबुद्धि का भी अभ्युदय यहीं होता है। यह प्रक्रिया दो दिशाएँ ले सकती है-पहली दिशा, जिसमें तर्कसंगति का उदय आत्म-संघर्ष की एक सुदीर्घ प्रक्रिया के भीतर से होता है। यहाँ बुद्धिवाद श्रद्धा का विलोम नहीं, बल्कि श्रद्धा से ही प्रेरित-परिचालित होता है। यह श्रद्धा पारंपरिक संस्थाओं के प्रति होती है जिनके माध्यम से भावनाएँ पारदर्शी आदर्शों के रूप में गहराती हैं। इसके विपरीत दिशा वह है जिसमें यह सरलीकरण एक सतही और बिना जोखिम के, निखरी, निहायत ही कामचलाऊ यांत्रिक समझ द्वारा किया जाता है।
14. कुछ विदेशी आदर्श हमारे अपने आदर्शों से साम्य रखते हैं। वे एक विजातीय मुहावरे में अभिव्यक्त वैकल्पिक प्रतिमानों की तरह हमें भा सकते हैं। पर उस मुहावरे को हम अपने धार्मिक प्रतीकों की तरह नहीं महसूस करते। दूसरी ओर, वे विदेशी आदर्श होते हैं जो हमारी परिस्थिति पर कदापि लागू नहीं होते। यहीं पर हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद से और मिथ्या देशाभिमान से ऊपर उठने की ज़रूरत होती है। यदि सचमुच कोई आदर्श हमारे अपने पारंपरिक आदर्शों के ही एक सरलतर और गहनतर प्राकट्य की तरह हमें अनुभव होता है, तो उसे महज इसलिए स्वीकार करने से इनकार करना कि वह विदेशी धरती में उपजा था-गलत होगा।
15. तर्क अथवा धर्म की सार्वभौमता की दुहाई देना ठीक नहीं है। सार्वभौम केवल ‘स्पिरिट’ है। हमारे अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा और दूसरे आदर्शों के प्रति एक उदार खुलापन। नई श्रद्धा को उपलब्ध करने का एकमात्र मार्ग पुरानी श्रद्धा को गहरा करने की क्रिया से ही गुज़रता है। यह धारणा बेबुनियाद है कि आध्यात्मिक जगत् में प्रगति का अर्थ एक तटस्थ तर्कबुद्धि द्वारा प्राचीन ईश्वर और नए ईश्वर के बीच निर्णायक तौर पर चुनाव कर लेना होता है।